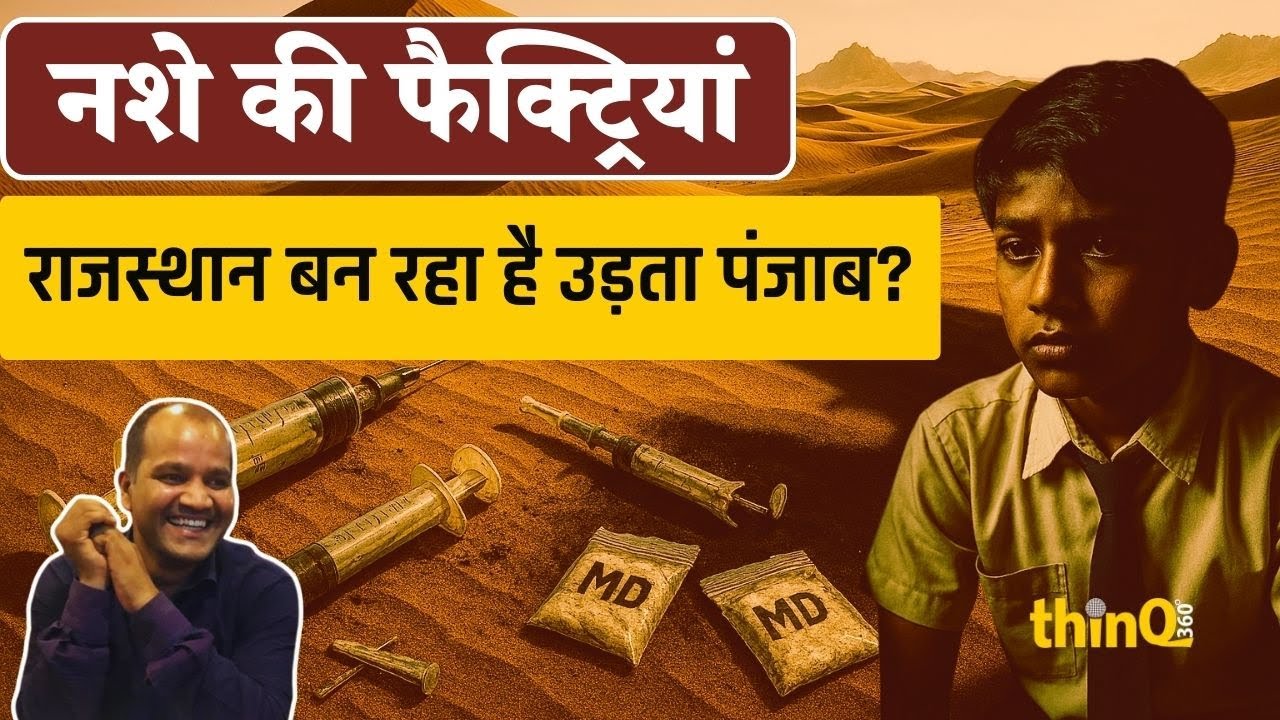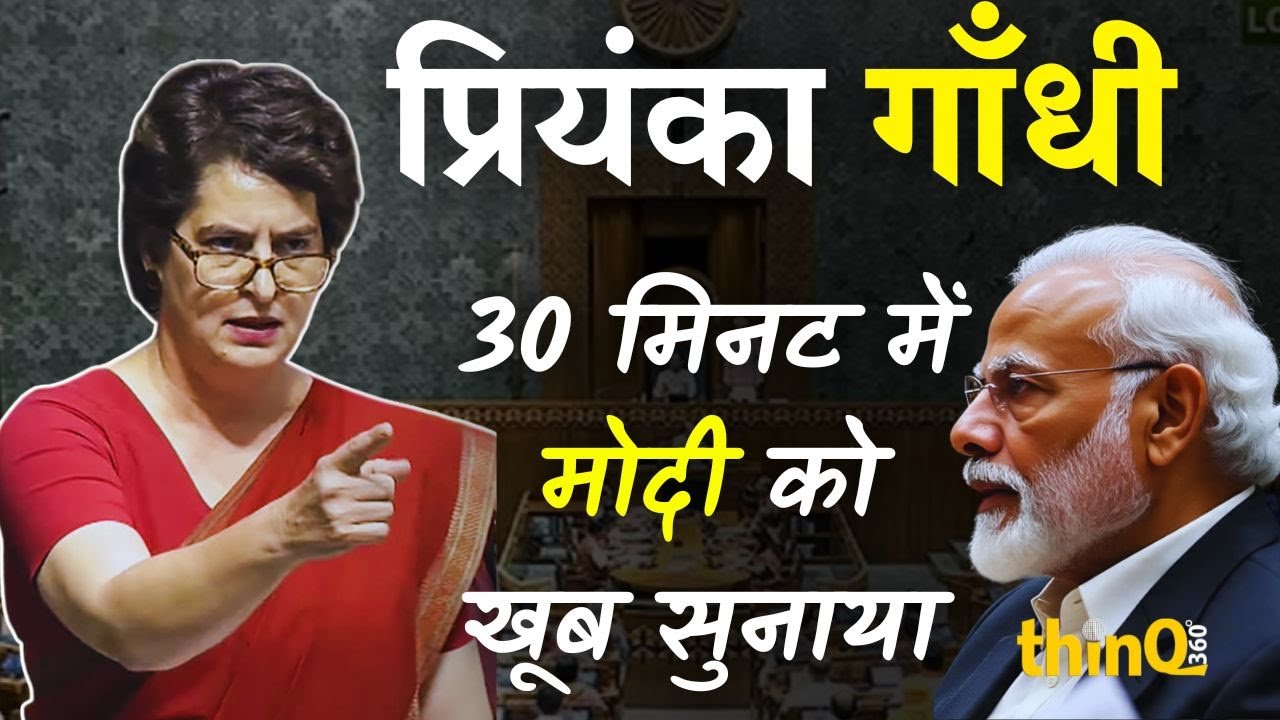जयपुर, 16 अगस्त 2025।
राजस्थान — वीरों की धरती, संस्कृति और रंगों का प्रदेश, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी चुनौती से जूझता इलाका। यहाँ की मिट्टी सदियों से प्यास का बोझ ढोती रही है। थार के विशाल रेगिस्तान से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक, हर कण में पानी की कमी की कहानी छुपी है।
आज भी राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल है, जहाँ पानी का संकट जीवन-मरण का प्रश्न बन चुका है। औसतन 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश, सूखती नदियाँ, टूटते-बिखरते तालाब और पलायन करते लोग — यह तस्वीर आम हो गई है।
बढ़ता संकट – थार की प्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि भारत के पास दुनिया के मीठे पानी का मात्र 4 प्रतिशत है। ऐसे में राजस्थान का हिस्सा कितना होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है।
बढ़ते तापमान और बदलते मानसून ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। चंबल, बनास, साबरमती जैसी नदियाँ घट रही हैं। दूसरी ओर खनन और बेतरतीब शहरीकरण ने भूजल को बुरी तरह प्रभावित किया है।
गाँवों में लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई भी पानी ढूँढने की मजबूरी में छूट जाती है।
आसमान से उम्मीद – ड्रोन से बारिश
इन हालातों के बीच हाल ही में जयपुर में हुई एक अनोखी पहल ने चर्चा बटोरी। यहाँ पहली बार ड्रोन के ज़रिए कृत्रिम बारिश कराने (क्लाउड सीडिंग) का प्रयोग किया गया। उद्देश्य था रामगढ़ बांध को भरना और जयपुर के आसपास के जल संकट को कम करना।
इस तकनीक में बादलों में सिल्वर आयोडाइड, नमक या ड्राई आइस जैसे रसायन छोड़े जाते हैं, जिससे पानी की बूंदें बनती हैं और बारिश की संभावना बढ़ती है।
भारत में क्लाउड सीडिंग नया नहीं है। 1951 में टाटा समूह ने पश्चिमी घाट में यह प्रयोग किया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में भी इसका इस्तेमाल सूखा कम करने के लिए हुआ।
लेकिन जयपुर में ड्रोन का प्रयोग पहली बार किया गया। यह हवाई जहाज़ की तुलना में सस्ता और सटीक माना गया। हालांकि, पहली कोशिश असफल रही। भीड़ और नेटवर्क ओवरलोड के कारण ड्रोन का जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर पाया और वह गिर पड़ा। इसके अलावा प्रशासन ने 400 फीट तक उड़ान की अनुमति दी, जबकि बादल 2000 फीट पर थे। अब वैज्ञानिक 10,000 फीट तक की मंजूरी माँग रहे हैं।
फायदे और खतरे
अगर यह तकनीक सफल हो जाए तो बारिश 18–25 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, फसल को सहारा मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन खतरे भी कम नहीं —
- रसायनों का असर पेड़-पौधों और पशुओं पर पड़ सकता है।
- प्राकृतिक चक्र में असंतुलन हो सकता है।
- गलत अनुपात से फसलों को नुकसान तक पहुँच सकता है।
अतीत की गूँज – परंपरा का ज्ञान
राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसका पारंपरिक जल ज्ञान रहा है। सदियों पहले यहाँ के लोग बावड़ी, झलारा, टांका, खड़ीन और कुंड जैसे अद्भुत जल-संरक्षण साधन बनाते थे।
- बावड़ियाँ – सीढ़ीनुमा संरचना, जहाँ गहराई में जाकर ठंडा पानी मिलता।
- टांके – छत से बरसात का पानी भूमिगत टंकी में जमा करने की पद्धति।
- खड़ीन – मिट्टी के तटबंध से खेतों में पानी रोकने का तरीका।
- कुंड – गहरे गड्ढे, जो दूर-दराज़ के इलाकों में भी जीवन का सहारा बनते।
ये सिर्फ़ जल स्रोत नहीं थे, बल्कि समाज का सामूहिक भरोसा थे। तब पानी को सिर्फ़ संसाधन नहीं, बल्कि पवित्रता और जीवन का आधार माना जाता था।
आज भी सरकार इन्हीं परंपराओं को आधुनिक रूप देने की कोशिश कर रही है — जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अमृत सरोवर जैसे अभियानों के ज़रिए।
भविष्य की जल लड़ाई
जल संकट सिर्फ़ राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय करेगा। आने वाले समय में पानी पर संघर्ष गाँव-शहर से निकलकर राज्यों और देशों तक पहुँच सकता है।
सवाल यही है कि क्या हम परंपरा और तकनीक का संतुलन बना पाएंगे? क्या बावड़ियाँ और ड्रोन साथ-साथ चल सकते हैं? क्या हम अतीत की सीख और भविष्य की तकनीक को जोड़कर एक सुरक्षित जल भविष्य गढ़ पाएंगे?
राजस्थान की प्यास एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि पानी प्रकृति की देन ही नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।
ड्रोन हों या बावड़ियाँ, तकनीक हो या परंपरा — पानी तभी बचेगा जब समाज मिलकर उसे बचाने का संकल्प लेगा। अगर आज हम सजग नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ़ प्यास ही विरासत में मिलेगी।
जल बचाइए, जीवन बचाइए।
 राजनीति
राजनीति