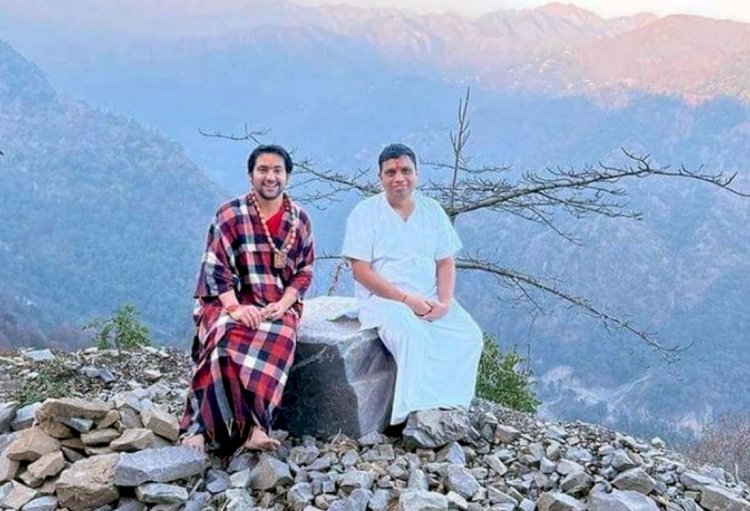Highlights
असलियत यह है कि प्रेमचंद के जूते फट तो गये थे बहुत पहले ही। हरिशंकर परसाई यह लिख भी चुके हैं। जो नहीं लिखा उन्होंने, वह यह है कि अब उन जूतों को कुतरने, उनकी चिंदी चिंदी उड़ा देने, उन्हें जड़मूल से मिटा डालने का खेल चल रहा है और यह खेल सुचिंतित और सुनियोजित प्रोजेक्ट है जिसमें पालिटिक्स न हो- ऐसा हो नहीं सकता।
निराला ने (मानसिक विचलन के दिनों को छोड़ कर) कब कहा था कि मैं हिन्दी का सबसे बड़ा लेखक हूं? प्रसाद ने कब कहा कि मुझे मान लो नंबर वन? यह कहने की बात नहीं होती है। यह बसने की बात होती है।
बहस, तर्क और सहमति- असहमति के बीच लगातार निष्ठुर होते हमारे समय के सबसे जरूरी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध सामने वाले से यह पूछना नहीं भूलते थे कि लगे हाथ अपना पंथ बता दो।
बता दो कि तुम्हारी रहगुजर क्या है और वह कहां तक जाती है। बता दो अपनी पालिटिक्स भी पार्टनर! यह मुक्तिबोध ही हैं जो नेमिचंद्र जैन तक को नहीं बख्शते: 'आपने एक नाजुक आदमी के साथ बड़ा ही बेरहम मजाक किया है। आपने उसे कवि बनाया।
दुर्धर्ष संघर्ष के उत्ताप से पीड़ित कवि।' मुक्तिबोध ने पालिटिक्स के पेशेनजर जो सवाल उस समय पूछा था, उसे बार बार पूछने का वक्त अब आ गया है और साहित्य की, रचनाकर्म की दुनिया में तो वह सवाल हमारे सर चढ़ कर बोल रहा है।
बोल ही नहीं रहा, हमारी घनघोर चुप्पी पर हमें पोर- पोर चीर भी रहा: 'मर गया देश, ज़िदा रह गये तुम!' यह सवाल जितना मौजूं है, उससे कहीं ज्यादा यह हमारे बचे और बने रहने का शिनाख्ती कार्ड है जिसे मिटाने की धुंआधार कोशिश में लोकलुभावन एक गोल अंधाधुंध चांदमारी कर रहा है। यह गोल कोई छोटामोटा गोल नहीं है। इसे तानपुरा बजाना भी आता है और बांसुरी बजाना भी... ।
समय, असमय, कुसमय- कभी भी। रोम जल रहा हो तो जले। सभ्यताएं मर रही हैं तो मरें। तालाब सूख रहे हों तो सूख जाएं। भूकंप और सैलाब आने हों तो आयें। हम इस नये संसार, उस नये संसार की इस नयी आमद को कौन सा नाम दें?
हम उसे साहित्य का नया पोप द्वीप समूह कहेंगे। इस नये पोप घराने को किसी भी किस्म की सूरतेहाल से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उसका मेघ मल्हार, उसके नक्षत्र, उसके नजूमी- सब अलग हैं। मुगालते में मत रहिए।
हालत यहां तक पहुंच गयी है कि प्रेमचंद जैसे बड़े रचनाकार के जूते तक में घुस आये हैं ये नये साहित्य उद्यमी और दावा कर रहे कि प्रेमचंद से बड़ी लकीर खींच दी है हिन्दी कथा संसार में संजीव ने। दावा ही नहीं कर रहे, गाल भी बजा रहे।
असलियत यह है कि प्रेमचंद के जूते फट तो गये थे बहुत पहले ही। हरिशंकर परसाई यह लिख भी चुके हैं। जो नहीं लिखा उन्होंने, वह यह है कि अब उन जूतों को कुतरने, उनकी चिंदी चिंदी उड़ा देने, उन्हें जड़मूल से मिटा डालने का खेल चल रहा है और यह खेल सुचिंतित और सुनियोजित प्रोजेक्ट है जिसमें पालिटिक्स न हो- ऐसा हो नहीं सकता।
यह खेल गांधी के किये- धरे के भी 'पोस्टमार्टम' के पीछे है, नेहरू के भी और भीमराव अंबेडकर के भी। यह खेल चतुर्दिक और बहुआयामी है, इसलिए मुक्तिबोध की जुबान में पूछना तो पड़ेगा इस कलाबाजी का राज।
जिन सज्जन ने यह पोस्ट फेसबुक पर डाली और उसे शेयर करने- कराने के गुरुतर दायित्व का निर्वाह किया, जिन्हें संजीव में प्रेमचंद से भी बड़ा रचनाकार दिखा- हम उन पर कुछ नहीं कहेंगे। इस तथ्य का जिक्र हम इसके पहले वाली अपनी पोस्ट में कर चुके हैं।
अब आगे का हाल अहवाल यह है कि उस दुर्धर्ष चिंतक की पोस्ट की भाषा से ( अगर वह किसी दूसरे से लिखवायी न गयी हो तो) लगता है कि कोई पढ़े- लिखे सज्जन हैं वह और यह करतब वह यूं ही नहीं दिखा रहे। कोई न कोई पालिटिक्स जरूर है..
कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी है...वरना ज़रूरत ही क्या थी इस किस्म के कुतर्क की? संजीव बड़े लेखक हैं तो होंगे। मानते रहिए आप। हम भी मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन वह प्रेमचंद नहीं हो सकते, वह रहेंगे संजीव ही और इसके पीछे बीसियों सहेतुक कारण हैं।
क्या प्रेमचंद को कभी लगा था कि उन्हें गोर्की या लूशुन से भी बड़ा रचनाकार यह दुनिया क्यों नहीं मान लेती? अरे भाई! प्रेमचंद, प्रेमचंद हैं, गोर्की, गोर्की हैं, लूशुन, लूशुन हैं। तीनों के कालखंड एक, चिंताएं एक जैसी, सरोकार एक जैसे- तो भी।
निराला ने (मानसिक विचलन के दिनों को छोड़ कर) कब कहा था कि मैं हिन्दी का सबसे बड़ा लेखक हूं? प्रसाद ने कब कहा कि मुझे मान लो नंबर वन? यह कहने की बात नहीं होती है। यह बसने की बात होती है।
हमारे- आपके दिलों में बसने की और प्रेमचंद को यह एजाज हासिल है तो सिर्फ उनकी अपनी रचनाओं की मार्फत जहां जीवन धड़कता है अपने पूरे के पूरे ताप- संताप के साथ। यह एजाज हिन्दी ही नहीं, इस देश की दीगर जुबानों में भी किसी और को हासिल हुआ हो और उसे प्रेमचंद जैसी स्वीकार्यता मिली हो तो नाम बता दें। हम अपनी बात वापस ले लेंगे। लेकिन प्लीज, पाप मोचन पत्र न बांटें।
आजादी के पहले इस देश का गांव कैसा रहा होगा, यह जानना हो तो किसी शहरातू को क्या करना चाहिए? उसे इतिहास पढ़ना चाहिए? हरगिज नहीं। उसे प्रेमचंद को पढ़ लेना चाहिए। काम खतम। फिर काहे की बेतुकी माथापच्ची कर रहे आप?
लालसा पैदा ही क्यों होती है कि हम अपने से पचास साल पुराने उस लेखक के जूते को कुतर डालें और ऐसे ताम्रपत्र गड़वाएं जिसमें प्रेमचंद जैसों के जिक्र तक की गुंजाइश न हो? हम प्रेमचंद की हत्या पर आमादा क्यों हैं?
हम क्यों चीरफाड़ में लगे हैं गांधी और नेहरू और अंबेडकर की? पालिटिक्स तो है साथी! यह पालिटिक्स ही गोडसे के लिए मंदिर बनवाती है और धीरेंद्र शास्त्री जैसों के लिए मीडिया मंच मुहय्या कराती है। पूछना तो पड़ेगा ही कि आखिर आपकी पालिटिक्स क्या है।
यह पालिटिक्स ही किसी को कुलपति बनने की राह दिखाती है तो किसी को ज़िदा मक्खी निगलने के फायदे समझाती है। यह पालिटिक्स ही तो है जिसमें सहिष्णुता के लिए अब रत्ती भर जगह नहीं बची। पहले मुक्तिबोध ने यह सवाल पूछा था, अब हम पूछ रहे, कल को कोई और पूछेगा।
 राजनीति
राजनीति